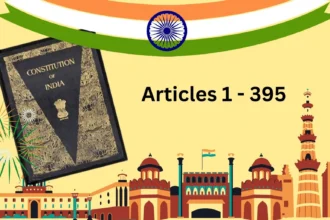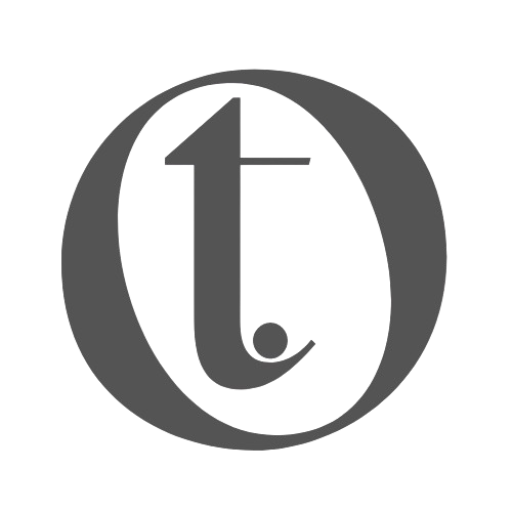अनुच्छेद 20 (Article 20 in Hindi) – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
[1] कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।
[2] किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
[3] किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यह अधिकार न केवल भारतीय नागरिकों को, बल्कि विदेशी नागरिकों और कानूनी संस्थाओं (जैसे कंपनियों) पर भी लागू होता है।
अनुच्छेद 20 के प्रमुख प्रावधान
1. पूर्व पद प्रभाव का कानून (Ex-post facto law)
- अभिशासन का सिद्धांत:
- कोई व्यक्ति तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने उस समय लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया हो।
- कोई व्यक्ति उस अपराध के लिए उस समय की निर्धारित सजा से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा।
- विशेषताएं:
- पूर्व पद प्रभाव का कानून वह है जो पहले किए गए कृत्यों को अपराध घोषित करता है या उनकी सजा को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के तहत ऐसा कानून अमान्य है।
- यह प्रावधान केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, न कि सिविल या कर कानूनों पर।
- करों या जन-उत्तरदायित्व के मामलों में इस प्रकार की सीमाएं लागू नहीं होतीं।
2. दोहरी क्षति से सुरक्षा (Double jeopardy)
- किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।
- यह सिद्धांत केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकरणों द्वारा लागू होता है।
- सीमाएं:
- यह प्रावधान विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई पर लागू नहीं होता क्योंकि वे न्यायिक प्रकृति के नहीं होते।
3. स्व-अभिशंसन के विरुद्ध सुरक्षा (Protection against self-incrimination)
- किसी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- यह अधिकार मौखिक और दस्तावेज़ीय साक्ष्य दोनों पर लागू होता है।
- सीमाएं:
- यह अधिकार भौतिक प्रमाण जैसे:
- अंगूठे के निशान।
- हस्ताक्षर।
- रक्त जांच।
- DNA परीक्षण।
- अन्य शारीरिक प्रमाण, पर लागू नहीं होता।
- यह प्रावधान केवल आपराधिक प्रकृति के मामलों पर लागू होता है।
- यह अधिकार भौतिक प्रमाण जैसे:
महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं
- पूर्व पद प्रभाव का सिद्धांत:
- यह सुनिश्चित करता है कि कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित न करे। उदाहरण: कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो पिछले वर्षों में किए गए कार्य को अपराध घोषित करे।
- दोहरी क्षति:
- यह केवल एक ही न्यायिक प्रक्रिया पर लागू होता है। अगर व्यक्ति को एक बार दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- स्व-अभिशंसन का अधिकार:
- यह अधिकार व्यक्ति को मानसिक यातना और अनैतिक दबाव से बचाने के लिए है।
- किसी व्यक्ति को गवाही के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20 के तहत निषिद्ध है।
अनुच्छेद 20 के उद्देश्य
- यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के सजा न दी जाए।
- न्यायपालिका को अधिक अधिकार देता है कि वह अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा कर सके।
- यह नागरिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अंग है और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है।
अनुच्छेद 20 का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को अनुचित और असंवैधानिक दंड से बचाना है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि दंड प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो और कानून के शासन का पालन हो।
Click here to read more from the Constitution Of India & Constitution of India in Hindi
Source : – भारत का संविधान