आदिवासी शब्द का मतलब होता है ‘मूल निवासी’। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं; और आज भी उसी तरह जी रहे हैं;। भारत की लगभग 8 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्त्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है।
[contents h2]
भारत में आदिवासी समूह
भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग-अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊँच-नीच का फ़र्क बहुत कम होता है इसी वज़ह से ये समुदाय जाति-वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं।
आदिवासी के धर्म
आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं; उनके धर्म इस्लाम, हिंदु, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अकसर अपने पुरखों की, गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएँ हैं। ये विभिन्न स्थानीं से जुड़ी होती हैं और इनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अकसर गाँव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता-कुंजों में पूजा की जाती है; जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है।
आदिवासी अपने आस-पास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आस-पास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मा पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएँ इसी के उदाहरण हैं। उन्नीसवीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण धर्म बन गया है।
आदिवासी के बोलने जाने वाली भाषाएँ
आदिवासियों की अपनी भाषाएँ रही हैं (उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवत: उतनी ही पुरानी हैं)। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी ‘ मुख्यधारा’ की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है।
आदिवासियों की उन्नीसवीं सदी में भूमिका
भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्त्व रहा है। लोहे, ताँबे, सोने व चाँदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी-बूटियाँ और पशु उत्पाद (मोम, लाख, शहद) और स्वयं जानवर (हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है), ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं;। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है; इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है।
उन्नीसवीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढँका हुआ था; और कम से कम उन्नीसवीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी-बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे; बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे।
आदिवासियों का विस्थापन
झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरीबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है;। उन्नीसवीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुँह में जा चुके थे।
आदिवासियों इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है;। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार-बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है; काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है; और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है।
सरकारी आँकड़ों से पता चलता है; कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं।
आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है; कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं; उनमें से 79 प्रतिशत आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बाँधों के जलाशयों में डूब चुकी है; पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है;। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क (40,501 वर्ग किलोमीटर) और 543 वन्य जीव अभयारण्य (1.18.918 वर्ग किलोमीटर) हैं; ये ऐसे इलाके है जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे।
विस्थापन से होने वाली परेशानियों और चुनौती
अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे-मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फँसते चले जाते हैं।
ग्रामीण इलाकों में 45 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 35 प्रतिशत आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं;। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं;। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है।
जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है; तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है; जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएँ और रीति-रिवाज गँवा देते हैं; जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है।
आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम
केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आस-पास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है;। इस कानून में यह भी कहा गया है; कि वन एवं जैवविविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है।
Related Links:

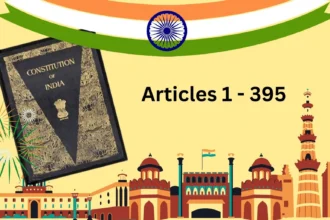
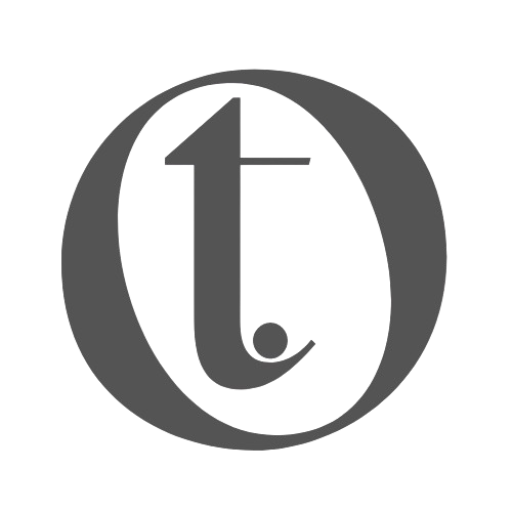
This is a best website
Thanks