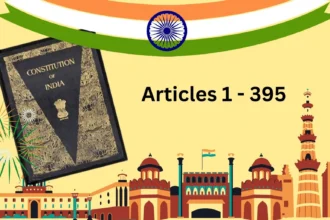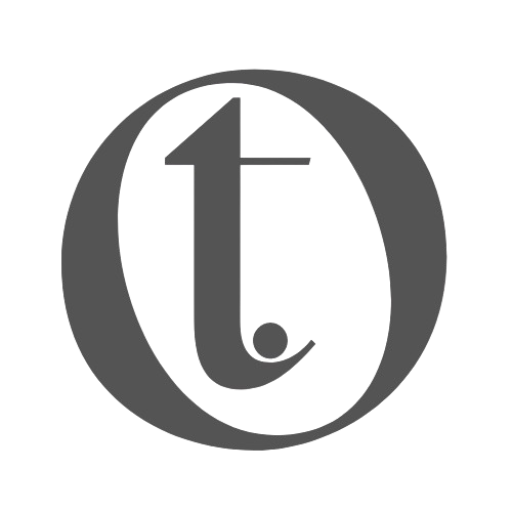विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए राज्य (राष्ट्र) आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देते हैं; इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं। इनका कार्य विधि में सुधार करना, अर्थात किसी न्यायप्रणाली में कानूनों की स्थिति की समीक्षा करना तथा कानूनों में परिवर्तन/परिवधन सुझाना है।
भारतीय विधि आयोग : परिचय
- भारतीय विधि आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है।
- आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिये होता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिये परामर्शदाता निकाय के रूप में कार्य करता है।
- इसके सदस्य मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं।
भारत में विधि आयोग का इतिहास
- भारतीय इतिहास में, विशेषकर पिछले 300 या इससे अधिक वर्षों के दौरान कानूनी सुधार एक सतत प्रक्रिया रहा है। प्राचीन समय में जब धार्मिक और प्रथागत कानून का बोलबाला था तो सुधार प्रक्रिया तदर्थ थी और उन्हें यधोचित रूप से गठित विधि सुधार एजेंसियों द्वारा संस्थागत नहीं किया जाता था।
- प्रथम आयोग 1833 के चार्टर ऐक्ट के अंतर्गत सन् 1834 में बना। इसके निर्माण के समय भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट एवं परस्पर स्पर्शी था तथा कुछ विधियों का स्वरूप भी भारत के प्रतिकूल था।
- द्वितीय आयोग की नियुक्ति 1853 ई. के चार्टर के अंतर्गत हुई। इसे प्रथम आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूपों, एवं न्यायालय तथा न्यायप्रक्रिया के सुधार हेतु आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का परीक्षण कर रिपोर्ट देने का कार्य सौंपा गया।
- तृतीय आयोग 1861 में निर्मित हुआ जिसमे मुख्यतः मौलिक दीवानी विधि के संग्रह का प्रारूप बनाना को प्रथम प्रारूप दिया गया। तृतीय आयोग की नियुक्ति भारतीय विधि के संहिताकरण की ओर प्रथम पग था।
- चतुर्थ आयोग कि नियुक्ति 1879 ई. में विटली स्टोक्स के अध्यक्षता में किया गया है। इसकी नियुक्ति पर सरकार ने एक आयोग इन विधेयकों की धाराओं का परीक्षण करने तथा मौलिक विधि के शेष अंगों के निमित्त सुझाव देने के लिए नियुक्त किया।
- भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि प्रथम चार विधि आयोगों का परिणाम हैं।
- भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 5 अगस्त 1955 को भारतीय संसद में घोषणा के साथ भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री मोतीलाल चिमणलाल सेटलवाड की अध्यक्षता में गठित किया। तब से 21 से अधिक विधि आयोग गठित किये जा चुके हैं जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष था।
- अब तक तीन-वर्षीय कार्यकाल वाले कुल 21 विधि आयोग गठित किये जा चुके हैं, जिनमें से 21वें विधि आयोग की कार्यावधि 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गई, लेकिन 22वें विधि आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है।
विधि आयोग के कार्य
- विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे संदर्भित या स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध या भारत में विद्यमान कानूनों की समीक्षा तथा उनमें संशोधन करने और नया कानून बनाने हेतु सिफारिश करता है।
- न्याय वितरण प्रणाली में सुधार लाने हेतु यह अध्ययन और शोध का कार्य भी करता है ताकि प्रक्रिया में देरी को समाप्त किया जा सके , मामलों का त्वरित निपटारा हो और मुकदमों के खर्च में कमी की जा सके।
- अप्रचलित क़ानूनों की समीक्षा/निरसन: ऐसे क़ानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक न हों और अप्रचलित तथा अनावश्यक कानूनों के निरसन की सिफारिश करना।
- कानून और गरीबी: गरीबों को प्रभावित करने वाले क़ानूनों का परीक्षण करता है और सामाजिक-आर्थिक विधानों के लिये पश्च लेखा-परीक्षा का कार्य करता है।
- उन नए क़ानूनों के निर्माण का सुझाव देता है जो नीति-निर्देशक तत्त्वों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में तय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं।
- न्यायिक प्रशासन: कानून और न्यायिक प्रशासन से सम्बद्ध किसी विषय, जिसे कि सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के मार्फत विशेष रूप से विधि आयोग को संदर्भित किया हो, पर विचार करना और सरकार को इस पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
- शोध: किसी बाहरी देश को शोध उपलब्ध कराने हेतु निवेदन पर विचार करना जिसे कि सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के मार्फत इसे संदर्भित किया हो।
- लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जाँच करना और उनमें संशोधन सुझाना।
- खाद्य सुरक्षा और बेरोज़गारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जाँच करना और वंचित वर्ग के लोगों के हितों के लिये उपाय सुझाना।
- समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और अनुसंधानों, जो कि इसके द्वारा लिये गए थे, पर रिपोर्ट तैयार करना और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना तथा ऐसी रिपोर्टों में ऐसे प्रभावी उपायों की सिफारिश करना जिन्हें केंद्र और किसी राज्य द्वारा अपनाया जाना है।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जिन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपा जाए।
- अपनी सिफ़ारिशों को ठोस रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय/विभाग और ऐसे अन्य हितधारकों से परामर्श करता है जिसे कि आयोग इस उद्देश्य के लिये आवश्यक समझे।
विधि आयोग में सुधारों की दरकार
20वें विधि आयोग के अध्यक्ष ए.पी. शाह ने विधि आयोग में कई सुधारों का समर्थन किया था, इनमें से प्रमुख हैं…
- Advertisement -
- इस निकाय को स्वायत्त एवं सक्षम बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इसे विधिक आयोग का दर्जा दिया जाए।
- अधिकांश देशों, विशेष रूप से पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में विधि आयोग एक विधिक निकाय है। यदि इस आयोग को विधिक दर्जा दिया जाता है तो यह केवल संसद के प्रति जवाबदेह होगा, न कि कार्यपालिका के प्रति।
- किसी भी आयोग की कार्यक्षमता में सुधार हेतु निरंतरता बेहद आवश्यक होती है। विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का है, प्रत्येक कार्यकाल की समाप्ति और अगले आयोग की नियुक्ति के मध्य काफी अंतराल होता है।
- 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हो गया था, किंतु 22वें विधि आयोग का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है।
- विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केवल अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात् ही की जानी चाहिये। वर्तमान व्यवस्था में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कई बार भेदभाव और पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं।
- वर्तमान व्यवस्था में विधि सचिव तथा विधायी विभाग के सचिव विधि आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इन आधिकारियों की आयोग में उपस्थिति इसकी स्वायत्तता को प्रभावित करती है।
- उपरोक्त आधिकारियों को इस आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिये। हालाँकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव होते हैं तथा विधि आयोग इस मंत्रालय के अधीन एवं सहयोग से कार्य करता है।
22वें विधि आयोग के गठन
केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसका गठन तीन साल के लिए किया जाएगा।
मुख्य कार्य
- ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब आवश्यकता या प्रासंगिक नहीं है और उन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है।
- मौजूदा कानूनों की जांच करेगा और सुधारों के लिए सुझाव देना है।
- संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों का व्यख्यान करना।
- कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर सरकार को अपने विचार देना और बताना जो कि विशेष रूप से कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ।
- केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके।
- किसी भी विदेशी देशों को अनुसंधान प्रदान करने के अनुरोधों पर विचार करें। जैसा कि सरकार द्वारा कानून और न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से इसे संदर्भित किया जा सकता है।